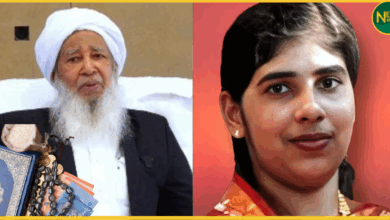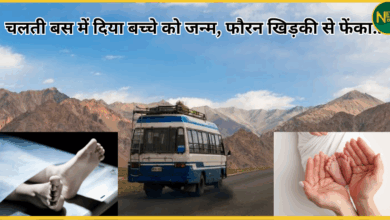हुक्का पार्लर में छापे का वीडियो वायरल, 15 हिन्दू लड़कियों और 15 मुस्लिम लड़कों के पकड़े जाने का दावा ?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि लखनऊ के एक हुक्का बार में 15 जुलाई 2025 को रेड हुई थी, जहां 15 मुस्लिम लड़के और 15 हिंदू लड़कियां पकड़ी गईं। इस वीडियो के साथ सांप्रदायिक रंग भी जोड़ा गया और इसे ‘लव जिहाद’ से जोड़ते हुए कई प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया गया। लेकिन फैक्ट चेक करने पर सामने आया कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है।
सच्चाई: ये वीडियो लखनऊ का नहीं, बल्कि 2022 का आगरा है
AI आधारित फैक्ट-चेकिंग टूल Grok (Twitter/X AI), The Quint, और India Today Fact Check की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो लखनऊ का नहीं बल्कि वर्ष 2022 में आगरा के एक कैफे में हुई पुलिस कार्रवाई का है। उस वक्त कैफे में कुछ हिंदू युवक और युवतियाँ हुक्का पीते हुए पाए गए थे। पुलिस ने उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा था। वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ना ही कोई सांप्रदायिक एंगल सामने आया था।
कैसे फैलाई गई अफवाह: पुराने वीडियो को नया बताकर भ्रम फैलाया गया
इस वायरल वीडियो को नए शीर्षक और मनगढ़ंत कैप्शन के साथ साझा किया गया, जिसमें लिखा गया कि “15 मुस्लिम लड़के और 15 हिंदू लड़कियां लखनऊ के हुक्का बार से पकड़ी गईं।” कुछ यूज़र्स ने यह तक कह दिया कि “सिर्फ हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़के क्यों?”, जिससे सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने की कोशिश हुई।
लखनऊ के हुक्का बार में कल पड़ी रेड में कुल 30 लोग पकड़े गये,15 लड़के 15 लड़किया। लड़कियां अच्छे खासे ऊंचे घरों की थीं। खास बात इसमें ये कि सभी#15 लड़के मुस्लिम थे, और सभी लड़कियां हिंदू घरों से थीं# एक भी मुस्लिम लड़की नहीं थी😲😠।
..इसपर ठंडे दिमाग से विचार करें… वरना जो… pic.twitter.com/eTcfz8vIYz— Pinki Bhaiya (@BHUPENDER_HRD) July 16, 2025
फैक्ट चेक रिपोर्ट: कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई धार्मिक पहचान नहीं हुई थी उजागर
फैक्ट चेकिंग एजेंसियों के मुताबिक:
- यह रेड 2022 में आगरा के एक कैफे पर हुई थी।
- वहां पाए गए सभी युवक-युवतियाँ हिंदू समुदाय से थे।
- किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
- वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देने की कोई सच्चाई नहीं है।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी
यह मामला एक बार फिर डिजिटल युग की चुनौती को सामने लाता है, जहां पुराने वीडियो और झूठे कैप्शन के ज़रिए समाज में भ्रम और नफरत फैलाने की साजिशें रची जाती हैं। हर नागरिक की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी भी वीडियो या खबर को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करें।
ये दावा झूठा, वीडियो पुराना और धार्मिक रंग देना खतरनाक
इस पूरी घटना का लखनऊ से कोई लेना-देना नहीं है। वायरल हो रहा वीडियो और उसमें किया जा रहा दावा पूरी तरह फर्जी है। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव फैलाना है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी किसी भी जानकारी को बिना पुष्टि के साझा करने से बचना चाहिए।
👉 नोट: News Nasha इस वायरल दावे को एक झूठी सूचना के रूप में प्रस्तुत करता है और किसी भी भ्रामक जानकारी को प्रमोट नहीं करता। हम पाठकों से अपील करते हैं कि वे तथ्यात्मक जानकारी पर ही भरोसा करें और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखें।